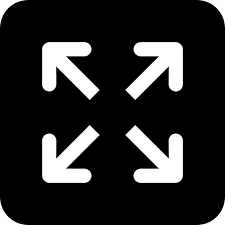ईसाई मिशनरियों की देन, गाँठ में जिनकी है ढेरों रुपैया

पिछले कुछ वज्रपातों में मैंने 'भारत की राष्ट्रभाषा का प्रश्नÓ उपस्थित करते हुए हिन्दी के अब तक राष्ट्रभाषा न बन पाने के कारणों को रेखाकिंत किया है। साथ ही, यह संकेत भी किया है कि हिन्दी ईसाई मिशनरियों के उपभोग का साधन ही बनी, किन्तु अतिउत्साह में हिन्दी प्रचार-प्रसार की बात करते हुए उपरोक्त तथ्य की जाँच-परख किये बिना ही हिन्दी के 'अन्धला गुरुÓ और 'निरन्ध चेलेÓ समय-असमय बहक (भटक) जाते हैं। और, प्राय: 'अन्धै अन्धा ठेलिया, दून्यूँ कूप पड़न्तÓ वाली स्थिति उपस्थित होती रहती है। ऐसे तथा अन्यान्य कारणों से राष्ट्रभाषा न बन पाने के सही सूत्रों पर आलोचकीय विवेक के साथ पड़ताल नहीं हो पाती। वास्तव में, हिन्दी के अतिआसक्त प्रेमी हिन्दी दिवस के अवसर पर जब 'जय हिन्दीÓ नारा लगाते हैं, वे उन जयकारों में प्राय: मिशनरियों के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट कर जाते हैं कि उन्होंने हिन्दी को सम्पूर्ण भारतवर्ष में पहुँचाया। ऐसी गोष्ठीधर्मी सतही चर्चा-परिचर्चाओं को देखते-सुनते हुए पुन: स्मरणीय है कि मिशनरियों ने हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के उद्देश्य से कदापि उसका प्रचार नहीं किया। उनकी साधना में ईसाइयत का प्रचार-प्रसार ही सर्वोपरि रहा है। उस साधना में, तत्कालीन समय में, हिन्दी एक साधन रूप में प्रस्तुत थी। हिन्दी अपनी साधन-रूपी अवस्था के कारण ही बाज़ार की भाषा बनी और शनै:-शनै: जन-मन की भाषा बनी।
ध्यानाकर्षण हो कि सिरामपुर मिशन से आरम्भ कर मिशनरियों का सांगठनिक विस्तार आज सम्पूर्ण भारत में है। पड़ताल करनी चाहिए कि आधुनिक काल में जिस हिन्दी गद्य की प्रतिष्ठा हुई, उसका सर्वाधिक लाभ किसने उठाया? ध्यान रहे कि 1800-1857 तक मिशनरियों ने अपना सांगठनिक विस्तार कर लिया था। इस विस्तार में हिन्दी और उसके गद्य स्वरूप की महती भूमिका थी। 1813 के चार्टर या ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के कारण व्यापारियों और मिशनरियों के लिए सारा भारत 'खुला बाज़ारÓ बन चुका था। यह तथ्य विस्मृत न हो कि तत्कालीन समय में भारत का बहुभाषी समाज किसी-न-किसी रूप में हिन्दी में भी व्यवहृत था। हिन्दी स्वाभाविक रूप में द्वितीय भाषा का कार्य निर्वाह कर रही थी। अत: मिशनरियों ने हिन्दी को सर्वपयोगी सहज सुलभ साधन के रूप में चुना और उसका लाभ उठाया। तथ्यत: हिन्दी का प्रसार उसके गद्य-वैविध्य के विकास के साथ उत्तरोत्तर हुआ।
प्रमाणित है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ही भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी। इसी मार्ग से मिशनरियों को प्रोत्साहन मिला। साम्प्रतिक समय में भी मिशनरी स्कूल सर्वाधिक चर्चित एवं अंग्रेज़ीपरस्त भारतीयों को इच्छित-अपेक्षित हैं। मिशनरी स्कूलों से ही उनका स्वप्न जगत् आलोकित होता है। अन्य (भारतीय) पाठशालाओं की अपेक्षा मिशनरी स्कूलों की सफलता के अनेकानेक कारण हैं, किन्तु एक बात रह-रह कर कचोटती है कि भारतीय पाठशालाओं का 'अन्यÓ (त्याज्य) हो जाना और 'वास्तविक अन्यÓ के साथ 'अनन्यÓ (आसक्ति) का भाव जुड़ जाना दीर्घकालीन सङ्घर्षोपरान्त स्वतन्त्रता अर्जित करने वाले भारतीय समाज में कैसे सम्भव हो सकता है? औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति की छटपटाहट में मिशनरी तथा कॉन्वेण्ट स्कूलों से मुक्ति की छटपटाहट क्यों नहीं है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्राय: सभी सरकारें इस अभियान में नाकाम सिद्ध हुई हैं। विस्मृत न हो कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ही भारत में मिशनरी स्कूलों की नींव पड़ी। इस अधिनियम में एक विशेष लक्ष्य केन्द्रित था - मिशनरियों को भारत में पहुँचाना और भारतीयों के कन्वर्जन में संलग्न होने की अनुमति प्रदान करना। उसमें निहित प्रावधानों के कारण ही भारत में रिलीजन के विस्तार के लिए 1814 में प्रथम बिशप के रूप में थॉमस फैनशॉ मिडल्टन की नियुक्ति हुई थी। उसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इस तथ्य के आलोक में उक्त अधिनियम को 'मिशनरी अधिनियमÓ भी कहा जा सकता है।
मिशनरियों के भारत आगमन में दो प्रमुख कारण थे। 19वीं शताब्दी के आरम्भ में नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण ब्रिटिशों की व्यापारिक स्थिति का डाँवाडोल हो जाना। इससे कुछ वर्ष पूर्व 1797 में एडम स्मिथ की पुस्तक 'वेल्थ ऑफ नेशनÓ प्रकाशित हुई थी, जिसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एक सिद्धान्त प्रतिपादित था, जो 'लाईसेस या लेज़ेज़ फेयरÓ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस सिद्धान्त का निहितार्थ था - निजी उद्योगों को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त रख कर ही आर्थिक विकास किया जा सकता है। 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत में 20 वर्षों तक व्यापार के लिए प्रदत्त एकाधिकार 1813 के अधिनियम के अन्तर्गत समाप्त किया गया और यहीं से व्यापारियों व मिशनरियों को भारत में निर्बाध प्रवेश की आधिकारिक अनुमति दी गयी। कृतज्ञता ज्ञापन की अबाध धारा का निर्वाह करते हुए अतिउत्साही हिन्दी प्रेमियों को मिशनरियों के हिन्दी प्रचार-प्रसार के लिए नेपोलियन बोनापार्ट के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, क्योंकि यदि तत्कालीन यूरोप उसके प्रभुत्वाधीन न होता, यदि वह महाद्वीपीय व्यवस्था जैसे राजनीतिक हथियार के उपयोग से ब्रिटेन की नाकेबन्दी न करता, तो हिन्दी अपने प्रचार-प्रसार से वंचित ही रह जाती। कहा जाता है कि नेपोलियन ने ब्रिटेन को 'दुकानदारों का देशÓ कहा था। और, केवल संयोग नहीं है कि एडम स्मिथ की पुस्तक ने उसे मुक्ति और आर्थिक विकास का मार्ग एकसाथ दिखाया। परिणामत: मिशनरियों का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार हिन्दी का प्रचार-प्रसार हुआ। भारत हिन्दी के माध्यम से मिशनरियों की सम्मोहक गुलामी में निमग्न हुआ।
ध्यान रहे कि ब्रिटिशों ने हिन्दी ही नहीं, अपितु प्राय: सभी भारतीय भाषाओं का साधन रूप में दोहन किया। आँकड़ेजीवी 'हिन्दी वालेÓ अत्यन्त उदारमना हैं। अत्यन्त मुग्ध होकर कहते हैं कि मिशनरियों ने हिन्दी का प्रचार-प्रसार किया। 1793 में विलियम कैरे भारत आया और उसने 'बाइबलÓ का बांग्ला में अनुवाद किया और 1909 में 'इंजीलÓ का 'नये धर्म नियमÓ शीर्षक से हिन्दी में अनुवाद प्रकाशित कराया। तत्पश्चात् मिशनरियों ने हिन्दी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं में ईसाई ग्रन्थों का अनुवाद प्रकाशित किया। पादरियों ने कई मिशनरी स्कूल आरम्भ किये। ईसाइयत की शिक्षा सम्बन्धी ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए सिरामपुर और आगरा में 'स्कूल बुक सोसायटीÓ आरम्भ की। प्रयागराज, काशी, सिकन्दराबाद और फर्रुखाबाद आदि स्थानों पर ईसाइयत के प्रचार हेतु छापखाने खोले। उनमें ईसा मसीह का गुणगान करने वाले ग्रन्थ, पाम्पलेट इत्यादि छपते रहे और मिशनरियों के प्रचार-तन्त्र के माध्यम से मुफ्त में वितरित होते रहे। समझिए कि 'दुकानदारों के देशÓ से आये पादरियों की 'गाँठ में ढेरों रुपैयाÓ था। उन्होंने रुपयों के बूते पर हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं को साधन बना कर ईसाइयत को भारत के प्रमुख धर्मों में स्थापित कर दिया। मिशनरी स्कूलों के छापखानों का ही अनुकरण है कि आज प्राय: सभी अंग्रेज़ी माध्यम के निजी स्कूल अपने-अपने मनचाहे पाठ्यक्रम-आधारित ग्रन्थ और नोटबुक (बहियाँ) छापते हैं। अन्तर केवल इतना है कि मिशनरियाँ अपनी प्रचार-सामग्री मुफ्त में वितरित करती थीं और आज अभिभावक मोटी रकम अदा कर निजी स्कूलों से पाठ्य-सामग्री और नोटबुक (बहियाँ) खरीदने के लिए विवश हैं। स्वीकारोक्ति यह भी कि इस अन्धाधुन्ध प्रक्रिया से मैं स्वयं भी छूटा नहीं हूँ। इस वर्ष दो-दो बार 'स्वर्णपत्रोंÓ पर प्रकाशित पाठ्य-सामग्री खरीदनी पड़ गयी। मरता, क्या न करता वाली स्थिति है। दुर्भाग्य कि हमारी सरकारें स्कूली शिक्षा को लेकर अभी भी सतर्क नहीं हो पायी हैं। और, अति उत्साही आँकड़ेजीवी हिन्दी वालों का तो क्या ही कहना, वे 'जय हिन्दीÓ के जयकारों में भारत की आत्मा की ही चिन्दी करने में निमग्न हैं। उनके लिए मिशनरियाँ महान हैं। इस प्रकार हिन्दी महान है।
(लेखक अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के संस्थापक हैं)