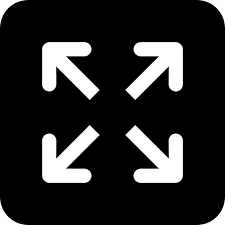पूर्ण भारतीय दर्शन की अनोखी खोज

अस्तित्व में दो नहीं। यहाँ द्वैत नहीं है। वेदांत अनुभूति में इसे अद्वैत कहा गया। ऋग्वेद के एक ऋषि ने इसे 'पुरुष' कहा और बताया कि जो भूतकाल में अब तक हो चुका और जो आगे होगा वह सब पुरुष ही है। पुरुष एक है। इसी के भीतर सम्पूर्णता है। यही बात ऋग्वेद में 'अदितिÓ के लिए कही गई है और छान्दोग्य उपनिषद में 'भूमा' के लिए। भूमा सम्पूर्णता का पर्याय है। पूर्ण भारतीय दर्शन की अनोखी खोज है। 'पूर्ण' असीम विराट है। संख्या गणित का विषय है। विराट अस्तित्व के रहस्य गणित की पकड़ में नहीं आते। गणित में बड़ी से बड़ी संख्या भी पूर्ण का ही भाग होती है। कोई भी संख्या पूर्ण से बड़ी नहीं होती। 'पूर्णÓ वैदिक पूर्वजों का आत्मीय विषय रहा है। 'शतपथ ब्राह्मणÓ उत्तर वैदिक काल का प्रमुख सामाजिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक व दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें संख्या व गणित के तमाम उल्लेख हैं लेकिन इसी के अंश वृहदारण्यक उपनिषद (पांचवें अध्याय) में पूर्ण की रम्य व्याख्या है। बताते हैं-'वह पूर्ण है, यह पूर्ण है-'पूर्णमद: पूर्णंमिदंÓ। मन प्रश्न करता है कि क्या पूर्ण भी दो हो सकते हैं। एक यह पूर्ण और दूसरा वह पूर्ण। इस जिज्ञासा का उत्तर भी इसी मंत्र में है-''यह पूर्ण उस पूर्ण का ही विस्तार है-पूर्णात पूर्णमुदच्यते।'' शंका तो भी शेष न रहे इसलिए आगे कहते हैं-''पूर्ण में पूर्ण निकाल देने पर भी पूर्ण ही बचता है-पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।'' भारतीय अनुभूति का यह पूर्ण उल्लासदायी है।
प्रगाढ़ अनुभूति और दर्शन में 'पूर्ण' पूरा पूर्ण है। हम सबको अनेक पूर्ण दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन उन्हें पूर्ण नहीं कहा जा सकता। जो वास्तविक पूर्ण है, उस पूर्ण में कुछ भी घटाओ, जोड़ो, गुणा करो, पूर्ण पूर्ण ही रहता है। नि:संदेह गणित में कोई भी अंश या संख्या पूर्ण से छोटी होती है लेकिन पूर्ण अनुभूति में अंश या संख्या भी पूर्ण ही होती है। सारी संख्याएं पूर्ण का ही अविभाज्य अंश हैं और अंश कभी पूर्ण से पृथक अस्तित्व नहीं रखते। इस दृष्टि से हम सब पूर्ण हैं। पूर्णता के बोध के अभाव में अपूर्ण जान पड़ते हैं। अपूर्ण होना दुख है, पूर्ण होना आनंद। वेदों में अनेक देवों की स्तुतियां हैं। पश्चिमी विद्वान इसी आधार पर भारतवासियों को बहुदेववादी बताते हैं। हम भारतवासी बहुदेववादी नहीं, बहुदेव उपासक हैं। ऋषि की घोषणा है कि इन्द्र, अग्नि तमाम देवता हैं लेकिन सत्य एक है, विद्वान उसे भिन्न भिन्न ढंग से बताते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं-''वह पुरुष और आदित्य में एक ही है।'' संभवत: कुछ विद्वान पुरुष को और कुछ सूर्य को अलग-अलग बताते रहे होंगे। ऋषि दोनों को एक बताते हैं। पूर्णता सनातन प्यास है। हम सब अपूर्ण हैं। भोजन या पानी की प्यास अपूर्णता का संदेश है। सांसारिक उपलब्धियों की इच्छा भी हमारी अपूर्णता की ही सूचना है। इच्छा, अभिलाषा या आकांक्षा अपूर्णता के ही बोधक हैं। तनावग्रस्त होने का कारण भी हमारी अपूर्णता है। हम अतृप्त हैं। हम किसी भी मार्ग या उपाय से समृद्धि चाहते हैं और समृद्धि अतिशीघ्र नई रिक्तता में बदल जाती है। सुख फिसल जाता है, दुख घेर लेता है। प्रकृति सृष्टि सम्पूर्णता है। सम्पूर्णता में ही रहती है। सम्पूर्णता में ही प्रकट होती है। यहाँ सामान्य गणित नहीं है। पूर्ण से पूर्ण घटा देने पर शून्य नहीं बचता। यहाँ अस्तित्व की सम्पूर्णता का सुन्दर विवेचन है-''मेरा मन ऐसा ही मंत्र गढ़ने को उतावला है-मैं अपूर्ण हूँ। हम सब अपूर्ण हैं। मैं में हम घटाओ तो अपूर्ण मैं ही बचता है।ÓÓ मैं दुख है, हम होना सुख है और सम्पूर्ण होना आनंद। सम्पूर्णता की प्यास स्वाभाविक ही गहरी ही होनी चाहिए। हम बोधरहित हैं सो अपूर्ण हैं। अपूर्ण हैं सो सांसारिक उपलब्धियों में पूर्णता खोजते हैं। सांसारिक उपलब्धियां क्षणभंगुर हैं। वे अपूर्ण से भी लघुतम हैं। हमारी अपूर्णता हमको बार-बार जगाती है। हम तनावग्रस्त होते हैं। अपूर्णता का ज्ञान अच्छा है। तब हम पूर्णत्व के बारे में विचार करते हैं। पूर्णता को प्राप्य मानते हैं। पूर्वजों ने शब्द संकेतों से ऐसा मार्ग दर्शन किया है। संसार के साथ स्वयं का ज्ञान ही पूर्णता की दिशा तय करता है।
कार्य और कारण की श्रंखला में पूर्ण विराम की गुंजाइश नहीं। 'ब्रह्म' पूर्णतम पूर्णता है। यह 'ब्रह्म' ही कारण है और 'ब्रह्म' ही कार्य। गीता के एक सुन्दर श्लोक (4.24) में 'ब्रह्म' ही 'ब्रह्म' को हवि अर्पण करता है-ब्रह्मार्पण ब्रह्म। 'ब्रह्म' ही अग्नि है और 'ब्रह्म' ही हवि। यह हवि 'ब्रह्म' को ही मिलती है। इसका परिणाम भी 'ब्रह्म' ही होता है। इसके पहले के श्लोक में ऐसा जानने वाले व्यक्ति के लिए ''ज्ञानावस्थित चेतस:-ज्ञान में स्थिर चेतना'' शब्द आए हैं। ऐसे व्यक्ति के सभी कर्म ''समग्रं विलीयते-सम्पूर्णता में विलीन होते हैं।'' लेकिन यह ज्ञान की उच्चतर स्थिति है। संसार का अध्ययन कार्य कारण की श्रंखला के विवेचन से होता है। संसार की प्रत्येक घटना के कारण होते हैं। ऐसे कारण के भी कारण होते हैं। कार्य कारण के प्रत्यक्ष सम्बंधों का अवसान सम्पूर्णता के बोध में ही होता है। हम संसार जानना चाहते हैं। इसलिए संसार विषय का ज्ञेय हुआ। जानकारी मिली यह ज्ञान हुआ। हमने जाना सो हम ज्ञाता हुए। लेकिन ज्ञाता और ज्ञान का सम्बंध भी अंत में समाप्त होता है। बोध के अंत में ज्ञाता नहीं बचता। ज्ञाता भी ज्ञान हो जाता है। ज्ञान भी अंतिम अवस्था में कहां बचता है? ज्ञाता, विषय, ज्ञान आदि सभी विभाजन सम्पूर्णता के ही भाग हैं। सम्पूर्णता का बोध भारतीय चिन्तन की अनूठी उपलब्धि है।
सत्य आधा नहीं होता। मित्रगण चर्चा में कहते हैं कि आपकी या हमारी बात 50 प्रतिशत सत्य है। कोई भी वचन प्रतिशत में सत्य नहीं होता। सत्य पूर्ण होता है। पूर्णता ही सत्य है और सत्य पूर्णता है। सत्य इससे कम नहीं होता। तैत्तिरीय उपनिषद में सत्यानुभूति की प्राप्ति के बाद का एक सुन्दर मंत्र है। मंत्र क्या खूबसूरत कविता है। ऋषि गाते हैं-''मैं अन्न हूँ। मैं अन्न हूँ। मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ। मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ।'' यहाँ अनुभूति का उल्लास है। इसलिए अभिव्यक्ति में दोहराव है। ध्यान देने योग्य बात है कि मैं स्वयं अन्न और मैं ही अन्न का भोक्ता। आगे कहते हैं-''मैं ही इन दोनों अन्न और अन्न के भोक्ता का संयोग कराता हूँ-अहम् श्लोककृतÓÓ फिर कहते हैं-''मैं ही ऋत सत्य हूँ। प्रथम उत्पन्न हिरण्यगर्भ हूँ। देवों से पहले हूँ। अमृत की नाभि हूँ-अमृतस्य नाभि:।ÓÓ पूर्ण में ही अन्न, अन्न का उपभोक्ता, ऋत सत्य सहित सम्पूर्ण अस्तित्व विद्यमान है। यही अनुगूंज गीता में भी है। कृष्ण कहते हैं-मैं सूर्य हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, आदि। पूर्वज पूर्ण में रहते थे। पूर्ण विराट है। उसकी असंख्य अभिव्यक्तियाँ हैं। हम उनकी गणना करने का प्रयास करते हैं। व्यावहारिक जगत् में ऐसा अनुचित भी नहीं है लेकिन पूर्ण का गणित नहीं होता। पूर्ण के भीतर ही गणित और अगणित है। व्याख्येय और अव्याख्येय भी हैं।
(लेखक उप्र विस के पूर्व अध्यक्ष हैं)