आत्मनिर्भर भारत की जरूरत है "मातृभाषा" में शिक्षा
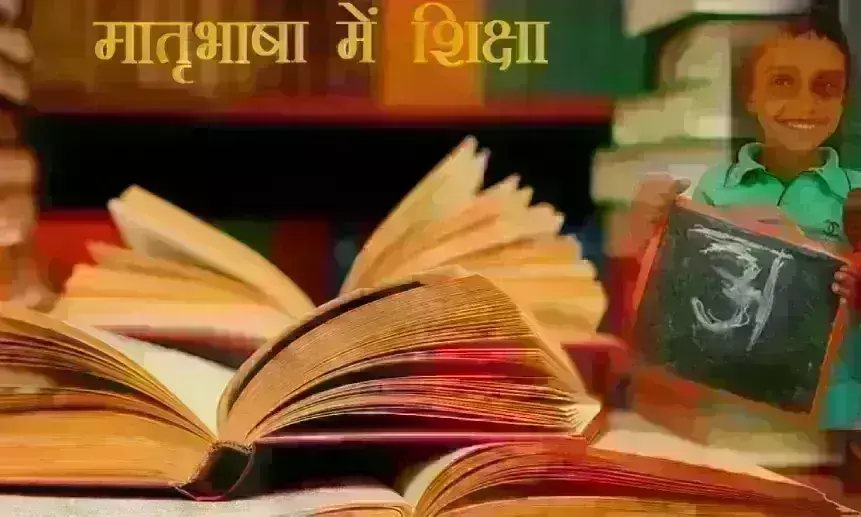
आज शायद ही किसी की इस बात से असहमति हो कि उच्च शिक्षा देश के सर्वतोमुखी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक निवेश है। उसी की सहायता से अनेक प्रकार की विविधताओं और विषमताओं वाले भारत में सबको सामर्थ्यवान बनाने की चुनौती का सामना किया जा सकेगा। शिक्षा के प्रभावी उपाय द्वारा इस लक्ष्य को साध पाने के लिए यह ज़रूरी होगा कि उच्च शिक्षा को अधिकाधिक समावेशी बनाया जाय ताकि उसकी पहुँच बढ़े और उसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। तभी सभी वर्गों को उन्नति का अवसर मिल सकेगा। शिक्षा देने के उपायों में भाषा का उपयोग सर्वविदित है क्योंकि ज्ञान प्रायः भाषा में ही निबद्ध होता है और उसके समुचित सहयोग लिए बिना शिक्षा की प्रगति प्रतिबंधित ही रहेगी। भाषा समाज की बिरासत और सम्पदा होती है जिसमें जीवन के सहज स्वर गूंजते हैं। यदि शिक्षा का आयोजन समाज की अपनी भाषा न हो कर कोई पराई भाषा हो ज्ञान पाने का काम दुहरी तिहरी कठिनाई वाला हो जाता है। उस अतिरिक्त भाषा को अपनाना एक अतिरिक्त काम हो जाता है जो समाज की मूल भाषा में व्यवधान भी डालता है और ज्ञान अर्जित करने के काम को अधिक कठिन बना देता है। इस दृष्टि से विचार करने पर उच्च शिक्षा के लिए माध्यम के प्रश्न पर विचार करते हुए हमारा ध्यान भारत की भाषाई विविधता पर जाता है जो देश की एक प्रमुख सामाजिक विशेषता है। यहाँ पर हज़ार से ज़्यादा भाषाएँ हैं जो विश्व के अनेक भाषा-परिवारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन भाषाओं का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है और इनके प्रयोग करने वालों की संख्या में बड़ी विविधता है। यदि प्रमुख भाषाओं की बात करें तो आज की स्थिति यह है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में २२ भाषाओं को अंकित किया गया है जो प्रमुखता से आज प्रयोग में आ रही हैं। हिंदी को वैधानिक राज भाषा का दर्जा मिला हुआ है और अंग्रेज़ी सह राज भाषा है।
उच्च शिक्षा का वर्तमान स्वरूप अंग्रेज़ी राज में औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य में शुरू हुआ था और किसी भारतीय भाषा की जगह विदेश की अंग्रेज़ी भाषा को उसके संचालन के लिए एकमात्र माध्यम के रूप में स्थापित किया गया। यह अंग्रेज़ी राज की सुविधा के लिए और उसकी साम्राज्यवादी सोच के अनुसार था। पश्चिमी ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हुए भारत में उसके प्रसार के लिए अंग्रेज़ी बड़ी मुफ़ीद साबित हुई। इस तरह भाषा और ज्ञान के विषय दोनों का ही आयात किया गया और यहाँ की उच्च शिक्षा की संस्थाओं को उसके अनुरूप ढाला गया। पठन-पाठन और मूल्यांकन आदि की पूरी व्यवस्था लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज़ पर अपनाई गई। कहना न होगा कि इस तरह की औपनिवेशिक व्यवस्था में अंग्रेज़ी भाषा के साथ-साथ पश्चिमी ज्ञान और संस्कृति का विस्तार भी भारत में हुआ। उसे प्रामाणिक, प्रासंगिक और उपयोगी कह कर इस तरह प्रचारित प्रसारित किया गया कि लोगों के मन में बैठ गया कि यही ठीक है। इसका स्वाभाविक परिणाम यहाँ की ज्ञान परम्परा और भारतीय भाषाओँ की सतत उपेक्षा के रूप में सामने आया। इस प्रक्रिया में भारतीय शिक्षा का भारत के साथ विलक्षण सम्बन्ध बना जिसमें भारत पश्चिमी ज्ञान के उपयोग की एक प्रयोगशाला बनता गया और देशज ज्ञान हाशिए पर जाता रहा या फिर उसे पश्चिमी ज्ञान के अनुकूल ढाला गया। इस तरह भारत के ज्ञान-केंद्रों पर ज्ञान-सृजन करने की जगह ज्ञान का अनुकरण और समायोजन का काम ही चलता रहा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ज़रूरी शैक्षिक समाजीकरण के अन्तर्गत अंग्रेज़ी सीखना, पश्चिमी ज्ञान देने वाले विषयों को सीखना और सुविधानुसार उसका उपयोग करना एक मानक काम बन गया। ऐसे में न केवल शिक्षा की जटिलता बढ़ गई बल्कि देश की प्रकृति की समझ भी बिगड़ती गई।विद्यार्थी पर शिक्षा का भार भी बढ़ गया। साथ ही एक हीनता की ग्रंथि का भी बीजारोपण हो गया। उसे सदा के लिए दूसरे की ओर देखना नियति बन गई। ग़ुलामी की मानसिकता इतनी प्रचंड थी कि आज भी कई स्कूल अंग्रेज़ी न बोलने और हिंदी जैसी भारतीय बोलने पर दंडित करते हैं। अंग्रेज़ी में गिटपिट बहुतों के लिए सुरक्षा कवच है तो बहुत लोग इसे रोब ग़ालिब करने का ज़रिया बनाए हुए हैं। आज भी कइयों के लिए अपनी विशिष्टता दिखाने और अलग पहचान बनाने के लिए अंग्रेज़ी एक मज़बूत वैसाखी बन खड़ी होती है। एक भाषा के रूप में अंग्रेज़ी का अपना महत्व और आकर्षण है जिसे सभी स्वीकार करते हैं। अंग्रेज़ी के अपने नाज़ औ नख़रे हैं, सौष्ठव है, असर है और वह बना रहे परंतु भारतीय भाषाओँ को विस्थापित कर अंग्रेज़ी मेम की जिस तरह तूती बोलती है वह किसी लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। भारत में भाषा की ग़ुलामी की दास्तान लम्बी हो चली है उसके दुष्परिणाम का आकलन सरल नहीं है। यहाँ इतना कहना ही काफ़ी होगा कि अपनी भाषा के स्वास्थ्य बनने और बिगड़ने के साथ विचार, आचार और पूरी संस्कृति भी बनती बिगड़ती है ।
भाषा-प्रयोग का एक पक्ष यह भी है कि भाषा की अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार है पर वास्तविकता कोसों दूर है। न्यायालय, विश्वविद्यालय, कार्यालय और रुग्णालय हर कहीं आज अंग्रेज़ी का ही वर्चस्व बना हुआ है। अलिखित रूप से भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्ति पर बंदिश और अंग्रेज़ी पर प्रलोभन का वातावरण चारों ओर व्याप्त हो रहा है। यह स्थिति सामान्य मानव अधिकारों के हनन को भी बखूबी व्यक्त करती है। हमें यह याद रखना होगा कि लोकतंत्र की मर्यादा है सबके लिए अवसर की समानता, समता, बंधुत्व और इन सबके लिए संवाद ही मुख्य आधार होता है। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा के साथ समाज में बड़े छोटे की दो कोटियाँ - अंगरेजीदाँ और ग़ैर अंग्रेज़ीदाँ की खड़ी कर दी गईं जिसके दूरगामी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम हुए जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाले सिद्ध हए। उससे उपजने वाली असुविधा और दुविधा पसरती गई और उससे अंग्रेज़ी की श्रेष्ठता और प्रामाणिकता को बल मिलता रहा। साथ ही सामाजिक जीवन में ऊँच नीच के भेद भाव और पूर्वाग्रह का भाषाई आधार स्वतंत्र भारत में दिन प्रतिदिन मज़बूत होता गया। लोकतंत्र में
शासक और शासित या प्रजा तथा राजा के बीच की दूरी कम होनी चाहिए थी पर वह बढ़ती रही। भारतीय संविधान भी मूलतः अंग्रेज़ी में ही तैयार हुआ। परीक्षाओं और नौकरी में अंग्रेज़ी को प्राथमिकता का रिवाज अभी भी प्रचलित है। इस माहौल में यही संदेश फैला कि भारतीय भाषाएँ विचलन हैं और मानक भाषा सिर्फ़ अंग्रेज़ी है। इसका दबाव भाषाओं में अस्वाभाविक दखल के रूप में उभरने लगा। भारतीय समाज और संस्कृति को देखने का देशज की जगह विदेशी नज़रिया प्रचलित हुआ और आधुनिक ज्ञान का विकास अपनी जड़ें उस तरह से न जमा सका जो होना चाहिए था।
चूँकि हमारा जीवन व्यापार ज़्यादातर भाषा की सहायता से ही सम्पादित होता है दुनिया के साथ उसका रिश्ता भाषा की मध्यस्थता के बिना अकल्पनीय है। इसलिए भाषा सामाजिक सशक्तीकरण के विमर्श में प्रमुख किरदार है फिर भी अक्सर उसकी भूमिका की अनदेखी की जाती है। वर्तमान सरकार देश को आत्मनिर्भर और स्वदेशी की दिशा मेनम आगे ले जाने के लिए कृतसंकल्प है। आत्म-निर्भरता के लिए ज़रूरी है कि अपने स्रोतों और संसाधनों के उपयोग को पर्याप्त बनाया जाए ताकि कभी दूसरों का मुँह न जोहना पड़े। कभी इस तरह की बातें ग़ुलाम देश को अंग्रेज़ी साम्राज्य की क़ैद से स्वतंत्र कराने और स्वराज्य स्थापित करने के प्रसंग में की ज़ाती थीं। अंग्रेज गए, स्वराज्य आया और देश में अपना शासन स्थापित हुआ। जनतंत्र में जिस लोकशाही की उम्मीद थी वह धीरे-धीरे बिखरती गई और राजा और प्रजा , शासक और शासित का भेद बढ़ता गया। शरीर तो भारत का रहा पर मन और बुद्धि अंग्रेज़ीमय या अंग्रेज़ीभक्त हो गया। भवसागर से मोक्ष के लिए हमने अंग्रेज़ी की नौका को स्वीकार किया और उसे शिक्षा तथा आजीविका का स्रोत बना दिया। अंग्रेज़ी से मुक्ति अंग्रेजों से मुक्ति से कहीं ज़्यादा मुसीबतज़दा और मुश्किल पहेली बन गई। मानसिक उपनिवेश बने रहने का सीधा परिणाम यह हुआ कि सृजनात्मकता प्रतिबंधित होती गई ।
वर्तमान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी की अवधारणा को विमर्श के केंद्र में लाकर सामर्थ्य के बारे में हमारी सोच को आंदोलित किया है। इसी कड़ी में नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अवसर देने पर विचार किया गया है। शिक्षा स्वाभाविक रूप से संचालित हो इसके लिए मातृभाषा में अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए । इसलिए बहुभाषिकता के आलोक में मातृभाषा का आदर करते हुए भाषा की निपुणता विकसित करना आवश्यक है। अमृत-महोत्सव के संदर्भ प्रधान मंत्री ने ग़ुलामी की मानसिकता से मुक्त होने के लिए आह्वान किया है और इसके लिए मातृभाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था ज़रूरी है।
